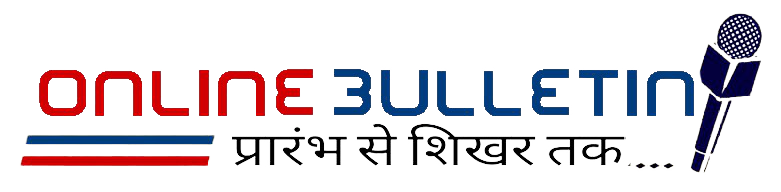क़ैदी परिंदा | ऑनलाइन बुलेटिन

©नीलोफ़र फ़ारूक़ी तौसीफ़, मुंबई
दफ़्न हैं कई राज़ तहख़ाने में,
डर है कहीं, सच से पर्दा उठाने में,
क़ैदी हैं जो बे-क़सूर आज भी,
कट गए हैं पंख, फड़फड़ाने में।
दबी हुई आवाज़ को जगाओ ज़रा,
लाखों हैं जेल में करो सुनवाई ज़रा,
न वकील न कोई जज है वहां,
ग़रीबी और बेबसी पे करो कार्यवाही ज़रा।
कोई चोरी, कोई बेक़सूर, कोई मुहब्बत,
झूठे इल्ज़ाम के क़ैदी को नहीं राहत,
गुजरूं जो कभी उस जेल से तो लगता है,
अब नहीं होगी इनपे कोई इनायत।
कोई बिछड़ा अपनों से, कोई बिछड़ा सपनों से,
कोई लुटा मज़हब के नाम, इंतज़ार रहा बरसों से,
बचपन में आया था, अब बुढ़ापा काट रहा है,
आंसू भी सुख गए, ख़ामोश लब लफ़्ज़ों से।
इंसानियत का हर दिन बजता है डंका,
दौलतवालों के शहर में मिलता है नंगा।
इसकी हर आवाज़ दब जाती है कहीं,
क़ैदी परिंदा सिर्फ़ लगता है भिखमंगा।
दर्द भी है, ग़म भी है आंसू की तहरीर भी,
झिंझोड़ रहा है देखो मुर्दा ज़मीर भी,
आग लगे जो दिल में ऎसी वो तहरीर हो
चलो बनाएं मुहब्बत की ऐसी तस्वीर भी।
चलो बनाएं मुहब्बत की ऐसी तस्वीर भी।